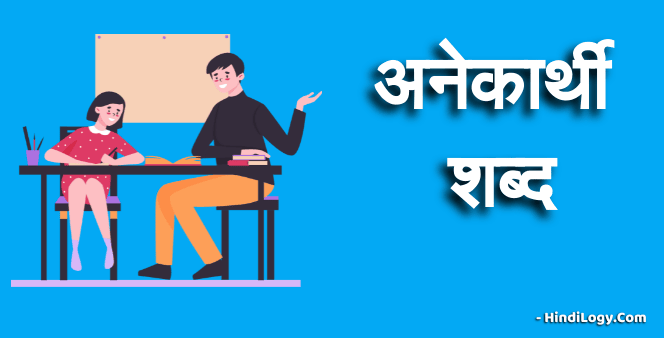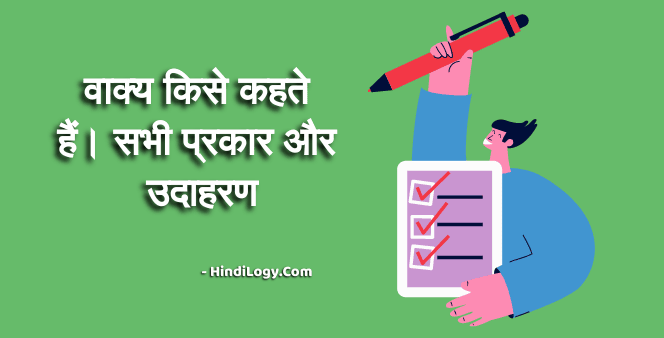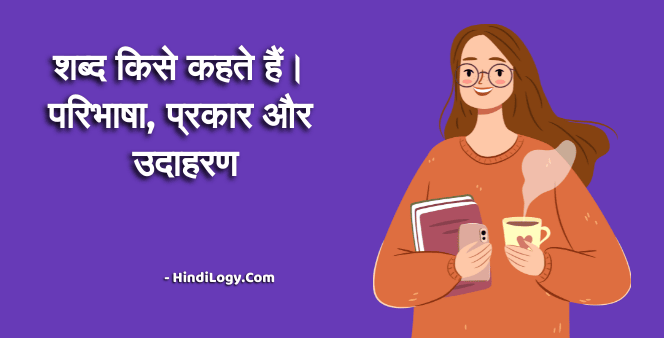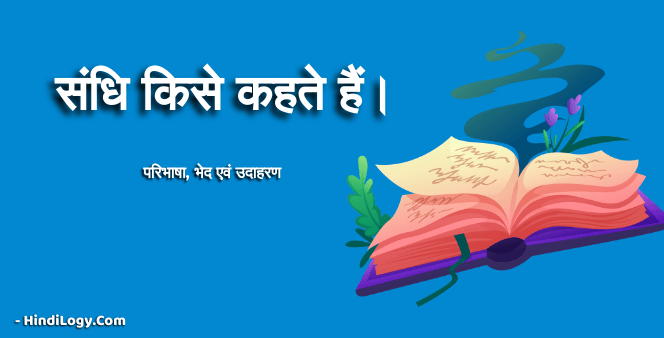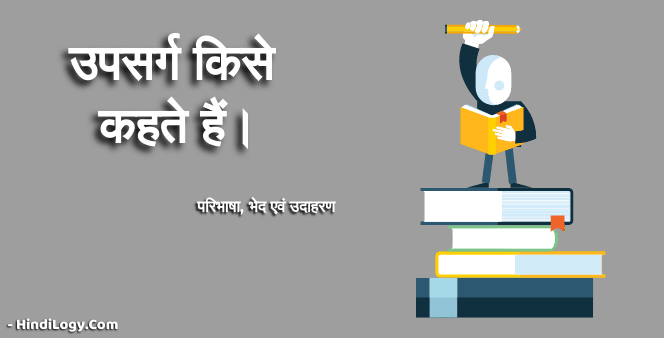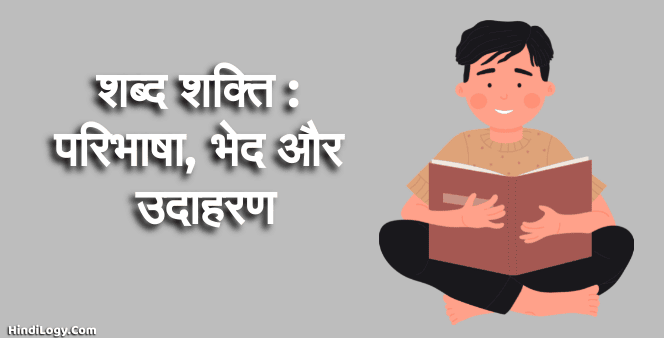
शब्द शक्ति – Shabd Shakti Kise Kahate Hain
शब्द शक्ति से अभिप्राय — शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग-अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है, तो उनके अलग-अलग अर्थ निकलते हैं।
इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द एवं अर्थ का अटूट और अभिन्न संबंध होता है। स्पष्ट है शब्द शक्ति का सामान्य अर्थ है — शब्दार्थ (शब्द एवं अर्थ का संबंध) संस्कृत काव्यशास्त्र में जिससे अर्थ की प्रतीति हो, उसे स्फोट कहा गया। शब्द और अर्थ दोनों की सामिस्टी को काव्य कहा गया।
शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण – संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक ‘काव्यप्रकाश’ के द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय के अंतर्गत तीन प्रकार के शब्द व तीन प्रकार की शब्द शक्तियां मानी जो निम्न प्रकार हैं –
[table id=10 /]
इनमें वाचक शब्द मुख्यार्थ का बोधक होता है। इसीलिए सबसे पहले उसे रखा गया है। लक्षक (लाक्षणिक) शब्द वाचक शब्द के ऊपर आश्रित रहता है।
इसलिए वाचक के बाद लाक्षणिक शब्द का स्थान रहता है। व्यंजक शब्द इन दोनों की अपेक्षा रखता है। इसीलिए उसको तीसरे स्थान पर रखा गया है।
शब्द शक्ति के भेद – Shabd Shakti Ke Bhed in Hindi Grammar
हिन्दी व्याकरण के शब्द शक्ति के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं –
(1) अभिधा शक्ति,
(2) लक्षणा शक्ति
(3) व्यंजना शक्ति
1 . अभिधा शब्द शक्ति
अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है – शब्द को सुनने/पढ़ने के बाद श्रोता (पाठक) को शब्द को लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होना। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है, जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता दौरा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है।
जैसे – परम रम्य आराम यहँ, जो रामहिं सुख देत।
यहाँ ‘आराम’ शब्द का अर्थ बगीची है। यह प्रकरण जनक की पुष्प वाटिका प्रसंग से है। ‘घोड़ा चर रहा है’ इस वाक्य में घोड़ा शब्द अपने मुख्य अर्थ का ही ज्ञान करा रहा है अतः इस वाक्य शब्द में अभिधा शब्द शक्ति ही काम कर रही है।
वाक्य/वाच्य/अभिधा शब्द के तीन प्रकार –
(क.) यौगिक शब्द – जिन शब्दों की व्युत्पत्ति होती है।
(ख.) रूढ़ शब्द – इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता।
(ग.) योगरूढ़ – दो शब्दों/शब्दांशों के योग से हुई रचना, ये सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताते हैं।
उदाहरण –
दैनिक जीवन में लोकव्यवहार हेतु प्रायः अभिधा शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यथा –
मोहन पढ़ रहा है।
सीता गा रही है।
बकरी चल रही है।
उपयुक्त वाक्यों में मुख्यार्थ ही प्रधान है। अतः अभिधा शक्ति हुई।
2 . लक्षणा शब्द शक्ति
‘लक्षणा’ शब्द की वह शक्ति है, जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट हो। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर तत्संबंधी विशेष/अन्य अर्थ को बताए तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति और उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं।
जैसे – बिहार जाग उठा।
यहाँ ‘बिहार’ शब्द का मुख्यार्थ है – भारत का एक राज्य। बिहार चेतनाहीन हैं जिसमें ये शक्ति नहीं है वह जग कर उठ खड़ा होगा। अतः बिहार का मुख्य अर्थ छोड़कर तत्संबंधी विशेष अर्थ लिया जाएगा — बिहार के निवासी।
स्पष्ट है प्रांत विशेष में रहने वाले लोगों में जोश उत्पन्न हो रहा है। इस तरह किसी व्यक्ति को देखकर ये कहना कि ‘अब शेर आया है।’ यहाँ शेर का अर्थ जानवर (मुख्य अर्थ) से न होकर वीर पुरुष (लक्ष्यार्थ) से है।
मम्मट के काव्य प्रकाश में उल्लेखानुसार लक्षणा शक्ति के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती है –
1 . मुख्यार्थ – बाह्य (रूढ़ा लक्षणा)
2 . लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध
3 . रूढ़ि (प्रयोजन/प्रयोजनवती लक्षण)
लक्षणा शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद हैं –
(क.) रूढ़ि/रूढ़ा लक्षणा – जहाँ पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ि अथवा परंपरा को आधार मानकर किसी वाक्य का अर्थ ज्ञात होता हो, वहाँ रूढ़ि/रूढ़ा लक्षना होती है।
जैसे –
1 . बिहार जाग उठा। इस वाक्य में (बिहार) से तात्पर्य बिहार में निवास करने वाले लोगों से है। अतः वाक्य का अर्थ होगा कि बिहार के निवासी सक्रिय हो गए हैं।
2 . बाजार में सन्नाटा है। यहाँ पर बाजार में सन्नाटा से तात्पर्य है कि बाजार में लोगों का आवागमन नहीं होने से चहल-पहल नहीं है।
(ख.) प्रयोजनवती लक्षणा – जहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा तो हो किंतु किसी प्रयोजन अथवा कारण को महत्व दिया जाए, वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन को महत्व दिया जाता है तथा मुख्य अर्थ गौण हो जाता है।
जैसे –
1 . गंगा में झोपड़ी है। प्रस्तुत वाक्य में गंगा में झोपड़ी होना असंभव है। अतः अर्थ होगा कि गंगा के किनारे झोपड़ी है। यहाँ पर मुख्यार्थ की अपेक्षा वाक्य के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अर्थ लिया गया है।
2 . शेर अब आया है।
3 . महेश तो निरा गधा है।
3 . व्यंजना शब्द शक्ति
जहाँ न वाच्यार्थ काम करें और न लक्ष्यार्थ अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करें और न ही तत्संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ व्यंजना शक्ति से शब्द का व्यंग्यार्थ लिया जाता है।
व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत मात्र देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता स्वयं लगाता है। काव्य में निहित गूढ़ अर्थ जिसे अभिधा/लक्षणा से नहीं जाना जा सकता वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
अनेकार्थक शब्द का एकार्थ में नियंत्रण करने वाले संयोगादि का अभिप्राय हैं –
1 . संयोग, 2 . वियोग, 3 . साहचर्य, 4 . विरोधिता, 5 . अर्थ 6 . प्रकरण, 7 . लिंङ्ग, 8 . सामर्थ्य, 9 . अन्य शब्द की सन्निधि, 10 . औचित्य, 11 . देश, 12 . काल, 13 . पुल्लिंग/स्त्रीलिंग रूप व्यक्ति और 14 . स्वर।
व्यंजना शब्द शक्ति के भेद –
(क.) शाब्दी व्यंजना – जहाँ पर व्यंगार्थ अर्थ पर आधारित न होकर शब्द पर आधारित हो, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है अर्थात शब्द विशेष के कारण व्यंगार्थ प्रकट होता हो, वहाँ पर उक्त शब्द शक्ति होती है।
जैसे –
‘ पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ‘ यहाँ पानी के अनेक अर्थ है और इसका पर्यायवाची रखने पर व्यंजना समाप्त हो जाएगी।
(ख.) आर्थी व्यंजना – शाब्दी व्यंजना के विपरीत इसमें जब शब्द बदल देने पर भी व्यंगार्थ निकलता रहे, तब आर्थी व्यंजना होगी। व्यंजना अर्थ में हो, किसी शब्द विशेष पर आधारित न हो। वहाँ आर्थी व्यंजना होती है।
जैसे –
एक मन मोहन तो बस के उजारियो मोहि,
हिय में अनेक मन मन मोहन बसावो ना।
हिंदी व्याकरण – Hindi Grammar
- हिंदी व्याकरण | वर्ण | स्वर वर्ण | व्यंजन वर्ण | शब्द | संधि | समास | उपसर्ग | प्रत्यय | संज्ञा | सर्वनाम | विशेषण | क्रिया विशेषण | वाक्य | लिंग | क्रिया | अव्यय | पुरुष | कारक | वचन | काल | विराम चिन्ह।
- अनेकार्थी शब्द | विलोम शब्द | पर्यायवाची शब्द | वाच्य | काव्य | तत्सम एवं तद्भव शब्द | अपठित पद्यांश | अपठित गद्यांश | पल्लवन | पद परिचय | शब्द शक्ति | पदबंध | रस | छंद | अलंकार।