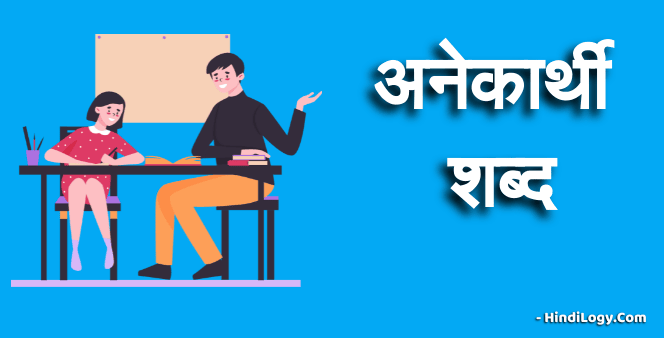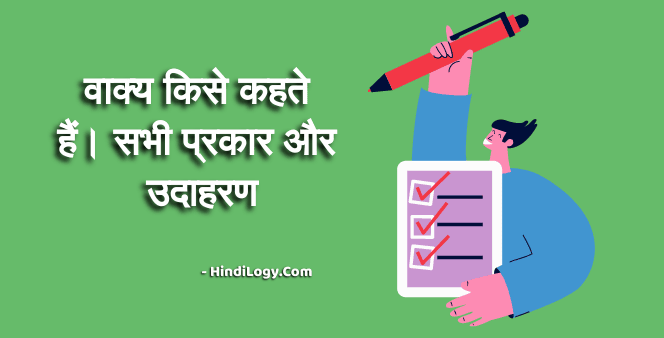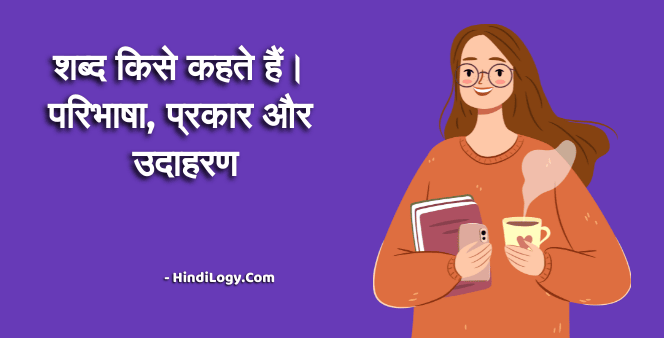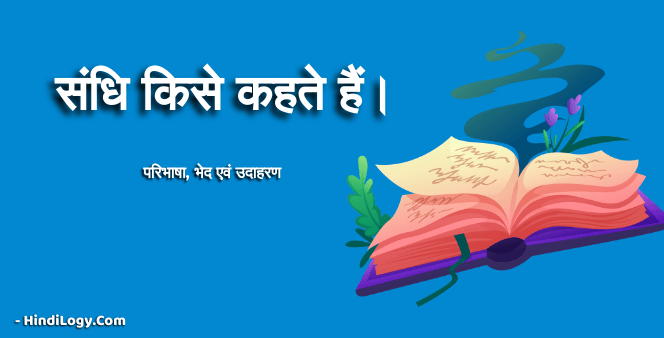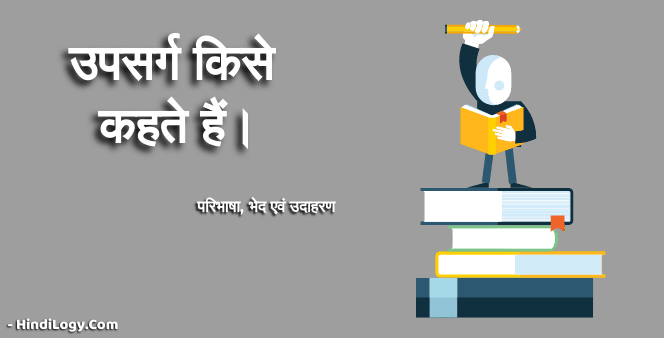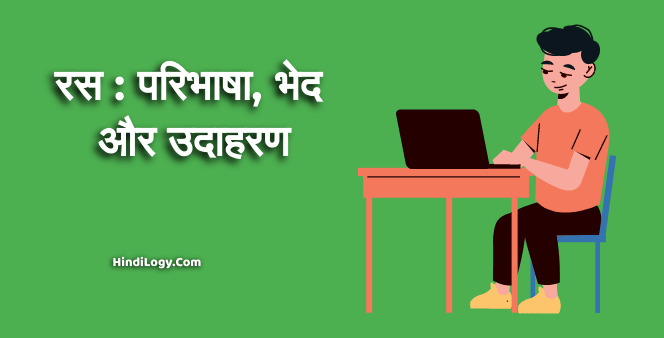
रस – Ras in Hindi Grammar
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादृसनिष्पत्ति:।
भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उक्त सूत्र को उल्लेखित किया है। सूत्र से स्पस्ट है की विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
रस किसे कहते हैं। – Ras Kise Kahate Hain
रस काव्य की आत्मा है। रस का शाब्दिक सामान्य अर्थ है – आनंद। काव्य को पढ़ते/सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं।
पाठक/श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से मिलकर रस रूप में परिणत हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने रस को काव्य का प्राणतत्व स्वीकार किया है।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार – “रस अखण्ड, स्वयं प्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेदांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्मा स्वाद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण होता है।”
रस के अवयव – रस के चार अवयव (अंग) होते हैं –
1 . स्थायी भाव – स्थायी भाव का अर्थ है प्रधानभाव। काव्य/नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। मूलतः 9 स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है।
रस और उनके स्थायी भाव –
रस — स्थायी भाव
1 . श्रृंगार रस — रति
2 . हास्य रस — हास
3 . करुण रस — शोक
4 . वीर रस — उत्साह
5 . रौद्र रस — क्रोध
6 . भयानक रस — भय
7 . वीभत्स रस — जुगुप्सा
8 . अद्भुत रस — आश्चर्य/विस्मय
9 . शांत रस – शम/निर्वेद/वैराग्य
2 . विभाव – स्थायी भाव के उदबोधक (उत्पत्ति) कारण को विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं –
(क.) आलंबन विभाव -जिसका आलम्बन (सहारा) पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं।
जैसे – नायक–नायिका।
आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं – आश्रयालंबन (जिसके मन में भाव जगे) एवं विषयालम्बन (जिसके कारण भाव जगे)
(ख.) उद्दीपन विभाव – जिन वस्तुओं (परिस्थितियों) को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है।
जैसे – चांदनी, उद्यान।
3 . अनुभाव – मन के भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। भरतमुनि ने अनुभाव का लक्षण दिया ‘जो वाचिक (आंगिक) अभिनय के द्वारा स्थायीभाव को अभिव्यक्तिरूप अर्थ का बाहरी रूप में अनुभव कराता है, उसको अनुभाव कहते हैं।’
स्पष्ट है अलग-अलग रस को प्रकाशित करने वाले बाह्व व्यापर अनुभाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस में वे अलग-अलग होते हैं।
अनुभाव चार प्रकार के होते हैं –
(क.) कायिक – शारीरिक चेष्टाएँ, आलिंगन, चुंबन, कटाक्ष।
(ख.) वाचिक – स्वगत कथन।
(ग.) आहार्य – स्वेच्छा से की गई वेशभूषा और श्रृंगार।
(घ.) सात्विक – स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंपन, स्वरभंग, अश्रु, मूर्च्छा, वैवर्ण्य।
4 . संचारीभाव – मन में संचरण करने वाले (आने-जाने वाले) भावों को संचारी भाव (व्यभिचारी भाव) कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है –
( 1 ) हर्ष ( 2 ) त्रास ( 3 ) लज्जा ( 4 ) विषाद ( 5 ) चिंता ( 6 ) शंका ( 7 ) ग्लानि ( 8 ) गर्व ( 9 ) मोह ( 10 ) उग्रता ( 11 ) निर्वेद (धिक्कारना) ( 12 ) धृति (इच्छापूर्ति) ( 13 ) उत्सुकता ( 14 ) आवेग ( 15 ) दीनता ( 16 ) जड़ता ( 17 ) चपलता ( 18 ) श्रम ( 19 ) मति ( 20 ) विबोध ( 21 ) निद्रा ( 22 ) स्मृति ( 23 ) उन्माद ( 24 ) मद ( 25 ) स्वपन ( 26 ) आलस्य ( 27 ) वितर्क ( 28 ) अवहित्था (छिपाना) ( 29 ) अपस्मार (मूर्च्छा) ( 30 ) व्याधि (रोग) ( 31 ) मरण ( 32 ) अमर्ष (दुःख) ( 33 ) असूया (असहिष्णुता)
रस के भेद या प्रकार – Ras Ke Bhed in Hindi Vyakaran
1 . शृंगार रस
(क.) संयोग श्रृंगार ( ख.) वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस नायक-नायिका की मिलन अवस्था में होता है।
उदाहरण (संयोग रस) :-
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय।
साँह करे, भौंहनि हंसै, दैन कहै नटि जाए।
उदाहरण (वियोग श्रृंगार) :-
भूषण-बसन बिलोकत सिय के,
प्रेम बिबस मन, कम्प पुलक तन, नीरज नैन भरे पिय के।
सकुचत कहत, सुमिरि उर उमगत, सील, स्नेह-सुगुण-गन तिय के।
सबसे पहले मतिराम ने ‘शृंगार रस’ को रसराज कहा।
2 . हास्य रस
किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा, विचित्र वेशभूषा आदि को देखकर दर्शक के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है।
उदाहरण –
जेहि समाज बैठे मुनि जाई। ह्रदय रूप-अहमिति अधिकाई।।
तहँ बैठे महेश-गन दोऊ। विप्र-बेस गति लखई न कोऊ।।
3 . करुण रस
किसी प्रियजन/प्रियवस्तु के अनिष्ट/विनाश से हृदय को दुःख/क्षोभ होता है।
उदाहरण –
करहिं विलाप अनेक प्रकारा।
परिहिं भूमि तल बारहिं बारा।।
4 . वीर रस
शत्रु अपकर्ष, दीन, दुर्दशा आदि किसी कठिन कार्य, युद्धादि करने के लिए हृदय में उत्पन्न उत्साह का भाव।
उदाहरण –
कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया,
भरे समझ कर जिनको अपना था अपनाया।
तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि,
रण यह यज्ञ पुरोहित! ओ किलात! ओ आकुली!
5 . रौद्र रस
ललकार, अपमान, मानभंग आदि से जागृत क्रोध से चित्त में उत्पन्न क्षोभ रौद्र रस कहलाता है।
उदाहरण –
उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।।
6 . भयानक रस
किसी भयानक वस्तु, प्राणी का वर्णन सुनने आदि से हृदय में उत्पन्न भय नामक स्थाई भाव भयानक रस में बदलता है।
उदाहरण –
उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी।
चली आ रहीं फेन उगलती फन फैलाये व्यालों-सी।।
7 . वीभत्स रस
घृणित वस्तुएँ देखकर ह्रदय में उत्पन्न घृणा/ग्लानि से वीभत्व रस की उत्पत्ति होती है।
उदाहरण –
रिपु आँतन की कुँडली करि जोगिनी चबात।
पीबहिं में पागी मनो, जुवती जलेबी खात।।
8 . अद्भुत रस
विभिन्न चमत्कारी दृश्यों/घटनाओं/वस्तुओं को देखकर हृदय में उत्पन्न कौतुहल जनित विस्मयकारी भाव अद्भुत रस होता है।
उदाहरण –
दिखरावा निज मातहिं अद्भुत रूप अखण्ड।
रोम-रोम प्रति लागे कोटि-कोटि ब्रहांड।।
9 . शांत रस
सांसारिक, नश्वरता, वैराग्य भाव, ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान आदि शांत रस कहलाता है।
उदाहरण –
मन रे तन कागद का पुतला।
लागै बूँद बिनसि जाय छिन में,
गरब करै क्या इतना।।
10 . वात्सल्य रस
शिशु चेष्टाओं को देख उनके प्रति प्रकट किए जाने वाला भाव वात्सल्य भाव कहलाता है।
उदाहरण –
कबहुँ चितै प्रतिबिम्ब खंभ में लवनी लिये खवावत।
दूरि देखत जसुमति यह लीला हरखि आनंद बढ़ावत।।
11 . भक्ति रस
प्रभु के गुणगान महत्ता सुनकर ह्रदय का गदगद होना, भक्ति में लीन हो अश्रु निकलना आदि चित्त वृत्तियाँ भक्ति रस के अंतर्गत आती है।
उदाहरण –
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु
मीरां के प्रभु गिरधर नागर हरस-हरस जस गायो।
विशेष : –
(क.) नवरसों में वातसल्य और भक्ति रस नहीं आते, इन्हें शृंगार रस में निहित माना जाता है।
(ख.) भरत मुनि ने नाटक में 8 रस ही माने हैं। शांत रस वहाँ नहीं माना।
हिंदी व्याकरण – Hindi Grammar
- हिंदी व्याकरण | वर्ण | स्वर वर्ण | व्यंजन वर्ण | शब्द | संधि | समास | उपसर्ग | प्रत्यय | संज्ञा | सर्वनाम | विशेषण | क्रिया विशेषण | वाक्य | लिंग | क्रिया | अव्यय | पुरुष | कारक | वचन | काल | विराम चिन्ह।
- अनेकार्थी शब्द | विलोम शब्द | पर्यायवाची शब्द | वाच्य | काव्य | तत्सम एवं तद्भव शब्द | अपठित पद्यांश | अपठित गद्यांश | पल्लवन | पद परिचय | शब्द शक्ति | पदबंध | रस | छंद | अलंकार।